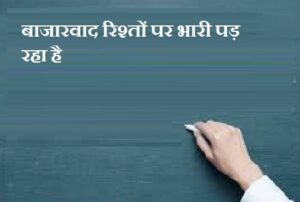
आज के उपभोक्तावादी समाज में हर चीज़ बेची जा सकती है और बेची जा रही है। कहते हैं बाज़ार का अपना कोई क़ानून नहीं होता. इसलिए, सभी चीजें, यहां तक कि मानवीय भावनाएं और रिश्ते भी, आनंद की वस्तु बन गए हैं। चाहें तो कीमत तय करके इसे खरीदा या बेचा जा सकता है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि समय के साथ परिवार, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। तेजी से बदलता समय इंसान की उम्र के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। बचपन को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्थिति कहां खो गई है या आज वैसी कोई स्थिति नहीं है। बच्चे सीधे युवावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं। अब बच्चे खिलौनों से नहीं, मोबाइल या कंप्यूटर से खेल रहे हैं। इसलिए वे समाज का हिस्सा नहीं बन सकते. वे किसी अदृश्य दुनिया में जा रहे हैं? कंप्यूटर गेम की दुनिया ने बच्चों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया है। अधिकांश किशोर कंप्यूटर गेम, सोशल मीडिया आदि पर अधिक समय बिता रहे हैं। यह बाजारवाद और उपभोक्तावाद अब परिवार और समाज पर भारी पड़ रहा है। बाज़ार का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। इसी कारण मानवीय भावनाएँ, रिश्ते-नाते, सुख-दुःख, आनंद सबका व्यवसाय होता है। इंटरनेट पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक जापानी अमीर आदमी ने रॉबर्ट कंपनी में निवेश किया है जो मानवीय भावनाओं को समझने और इंसान के अकेलेपन को खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। जो रॉबर्ट बन रहा है उसका नाम लोबर्ट है। जापान के अमीर आदमी के अनुसार, रॉबर्ट सभी मानवीय भावनाओं को समझ सकते हैं और लोगों को स्वस्थ और सक्षम रख सकते हैं। उनकी राय में रॉबर्ट ने कोरोना के दौरान मरीजों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई. यह भी सच है कि जब समाज में मनुष्य की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है या जब मनुष्य अपनी भूमिका से भटक जाता है तो मशीन की मदद की जरूरत पड़ती है। अब मुनाफ़े का बाज़ार व्यापक होता जा रहा है। यहां तक कि किसी व्यक्ति या इंसान के अंतरंग पल भी बाजार का हिस्सा बन गए हैं जो केवल उसके परिवार तक ही सीमित थे। निजी जिंदगी को बाजार में लाने में फिल्में और सीरीज भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब शादी से पहले पति-पत्नी महंगी साड़ियां और गहने पहनकर तस्वीरें (फिल्में) खिंचवा रहे हैं और जिस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं वह वास्तविक दुनिया से अलग पराया जेसे लगता है। आजकल मातृत्व (गर्भावस्था) की याद को बरकरार रखने के लिए मैटरनिटी फोटोशूट कराया जाते हैं। जैसे-जैसे सामान और सेवाएँ बेची जा रही हैं, भावनाओं का भी विपणन किया जा रहा है। मनुष्य क्षणिक सुख के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। इसके लिए लोगों को पैसे उधार लेने से भी हिचखिचता नेहीं । उपभोक्तावादी संस्कृति और बाजार का विस्तार आवश्यकता से अधिक चाहत और दिखावे पर जोर देता है। इसलिए बाजार की ताकतें बच्चे के सामने दिख रही संकट की स्थिति को व्यावसायिक अवसर के रूप में देख रही हैं। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं। इसी कारण बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सोशल मीडिया और कंप्यूटर गेम के कारण पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक गतिविधियों में बच्चों (बच्चों) और किशोरों की भागीदारी बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार,साल मे लगभग १००० हत्याएं, लगभग ७२५ अपहरण और ६००० से अधिक चोरी और डकैतियां बाल अपराध रेकड़ की गईं। खेलने और पढ़ने की उम्र के बच्चों और किशोरों इतने सारे अपराध करना चिंता का विषय होना चाहिए। मोबाइल गेम में बड़ी रकम गंवाने के बाद बच्चों और किशोरों घर से चोरी करने जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसा लगता है कि समाज अब बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गया है और ऐसी घटनाओं को असहाय होकर देख रहा है। दुर्भाग्य से शिक्षा ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। परिवार और स्कूल भी मूक दर्शक हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। परिणामस्वरूप, वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और समाज और देश के उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज की शिक्षा बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनाकर खड़ा करती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा जीतना ही उनके अस्तित्व की पहचान कही जाती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित होना आवश्यक है। ये सभी शिक्षण और कोचिंग सेंटर संगठन केवल माता-पिता की खर्च करने की शक्ति को देखते हैं, बच्चों की रुचि या योग्यता को नहीं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षाएं यह नहीं सिखाती कि जीवन किसी एक प्रतियोगिता तक ही सीमित है या प्रतिस्पर्धा जीवन का दूसरा नाम है, बल्कि स्वयं को जीतना ही जीवन है। कथित सामाजिक संकट के लिए परिवार भी काफी हद तक जिम्मेदार है। कई समाजशास्त्रियों का मानना है कि परिवार की अवधारणा में ऐसे तत्व हैं जो परिवार को असामाजिक बनाते हैं। महिलाओं के शोषण को वैध बनाना और महिलाओं को पारिवारिक माहौल से बाहर न जाने देने जैसी कई बातें हैं जो परिवार को असामाजिक बनाती हैं। विभिन्न विज्ञापनों और मीडिया में महिलाओं को सौंदर्य की वस्तु बनाकर बाजार का विस्तार तो किया जाता है और मुनाफा भी कमाया जाता है, लेकिन महिलाएं सशक्त नहीं हो पातीं। बाजार का चरित्र कल्याणकारी नहीं बल्कि व्यक्तिवादी है. इसलिए, बाजार के पास लाभ के लिए आय उत्पन्न करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। बाजार की ताकतें केवल लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए इससे बेहतर की उम्मीद करना व्यर्थ है। लेकिन एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य होने के नाते परिवार और शिक्षकों के इन चीजों से दूर रहने से समाज में कई तरह की अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। वर्तमान की स्थिति से ही भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। भविष्य कितना डरावना होगा ये बताने की जरूरत नहीं है. बाज़ार मानवीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं लेकिन ज़रूरतों से निर्देशित और नियंत्रित नहीं होते हैं। यदि बाजार जरूरतों को निर्धारित और नियंत्रित करेगा तो यह समाज और राष्ट्र के लिए खतरा पैदा करेगा।










